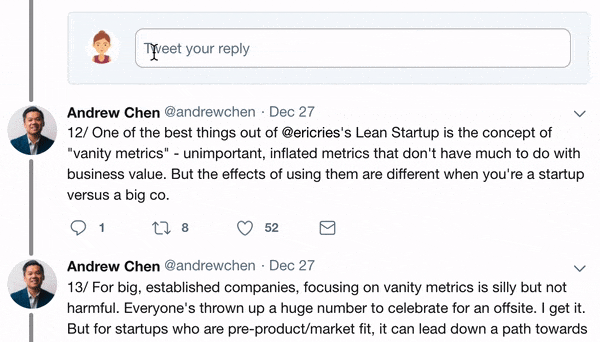थ्रेड: आदि-अनादि- 1
डिस्क्लेमर: ये पूरा फ़र्ज़ी थ्रेड है। फिलोसोफी का अपच है। हो सके तो इग्नोर करिये।
आजकल शिवभक्ति का काफी उबाल आया हुआ है। केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, तुंगनाथ से लेकर देश विदेश के भिन्न भिन्न कोनों में छुपे हुए शिवलिंग देखने को मिल रहे हैं।
डिस्क्लेमर: ये पूरा फ़र्ज़ी थ्रेड है। फिलोसोफी का अपच है। हो सके तो इग्नोर करिये।
आजकल शिवभक्ति का काफी उबाल आया हुआ है। केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, तुंगनाथ से लेकर देश विदेश के भिन्न भिन्न कोनों में छुपे हुए शिवलिंग देखने को मिल रहे हैं।
आधुनिक पीढ़ी का शिव के साथ ये प्रेम देखकर थोड़ा आश्चर्य सा होता है। आश्चर्य इसलिए क्यूंकि दोनों बिलकुल ही विपरीत प्रवृति के हैं। आधुनिक पीढ़ी के पास आराम की सारी ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जिनके बारे में सौ साल पहले कोई सोच भी नहीं पाता था।
गर्मी में AC, सर्दी में हीटर, सीढ़ी चढ़ने के लिए लिफ्ट, घूमने के लिए गाडी, एक से बढ़कर एक गैजेट, मनोरंजन के इतने साधन हैं कि कंफ्यूज हो जाएँ। दूसरी तरफ शिव हैं, बर्फ से पूरी ढकी पहाड़ के चोटी पर आधा शरीर ढके हुए, पशुओं के सानिध्य में, बिना घर बिना छत के वैरागी जैसे बैठे रहते हैं।
दोनों जीवन शैली के चरम छोर जैसे प्रतीत होते हैं। फिर क्यों शिव से मिलने की इतनी इच्छा है? और जितनी दुर्गम जगह पर शिवलिंग होगा उसका क्रेज उतना ही ज्यादा। मेरे जैसे कई लोगों का तो रिटायरमेंट प्लान ही है कि सारी सुख सुवधाओं को आग लगाकर किसी सुदूर जंगल या पर्वत की घाटी में रहा जाएगा।
प्रकृति की गोद में, शिव के पास। हमारे पूर्वज भी ये देख के सर पीट लेते होंगे कि उन्होंने तो इतनी मेहनत करके इतने बड़े बड़े नगर बसाये, इतनी सुविधाएँ जुटाई, और एक हम हैं जिनको फिर से जंगल-पहाड़ों में बसना है। जहां न इंटरनेट है, न गाडी जाती है, खाने को न स्विगी है न जोमैटो।
मानसिकता में ये परिवर्तन अकारण तो नहीं लगता। वरना 'शिवभक्तों' की तादाद इतनी मात्रा में ना बढ़ती। कहीं न कहीं ये दोनों छोर आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय दर्शन भी तो समय की चक्रीय गति को मानता है। तभी तो सबसे नवीन पीढ़ी सबसे पुरातन आदिपुरुष की ओर आकर्षित हो रही है।
कहीं न कहीं हमारी सर्वसुविधा संपन्न आधुनिक जीवन शैली में कुछ रिक्ति है। भौतिकता का तो विकास हुआ है, मगर कुछ न कुछ पीछे छूट गया है। शायद उसी को लेने शिव के पास वापिस जा रहे हैं हम।
Contd...
Contd...
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh